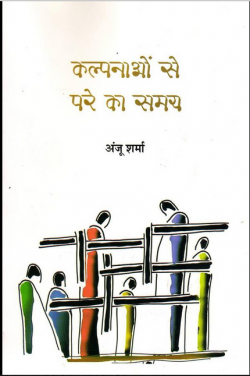कल्पनाओं से परे का समय / अंजू शर्मा / पृष्ठ-1
समीक्षा:मदन मोहन कंडवाल
पुस्तक: कल्पनाओं से परे का समय
रचनाकार: अंजू शर्मा
प्रकाशक: बोधि प्रकाशक समूह नई दिल्ली
मूल्य: 90 रुपये
कविताकोश पर पुस्तक
"कल्पनाओं से परे का समय " अंजू शर्मा जी के कविताओं का संग्रह जो कि बोद्धि प्रकाशन में मुद्रित होकर फरवरी में संपन्न विश्व पुस्तक मेले में लोकार्पित हुआ है, सचमुच सहज ही पाठक द्वारा बिना भूमिका बांधे भी, पढने के काबिल है। अंजू जी के शब्दों में ही- कविता उनके लिए मुक्ति और सद्गति का आवाह्न लिए हुए है। आस्था और विश्वास का सुरसंगम है। आधी आबादी का विमर्श और उसमे लेशमात्र कहीं भी आत्ममुग्धता नहीं होना भी काबिले तारीफ है। कविता में साम्य मुख्यतया तीन प्रकार का माना गया है। सादृश्य , साधर्म्य (दोनों संयुक्त रूपेण प्रभाव साम्य के नाम से चर्चित)और मात्र शब्दसाम्य। अंजू जी की कविताओं में प्रभाव साम्य की प्रचुरता निः संदेह प्रशंशनीय है।
बेटी के लिए मान के अंतस से उद्गमित कामानएं हर किसी माँ की अनुभूति को शब्दों का जमा पहनाने सी है। हाथ कंगन को आरसी क्या स्वयं ही परिलक्षित हो रहा है यथा "बेटी" ;
मै चुपके से पकड़ा देती हूँ तुम्हारे हाथ में कुछ चेतावनी भरी पर्चियां (गिरगिटों श्रीगालों लोमड़ भेड़ियों से बचने का आगाह )/
सीने की गहराइयों में तुम्हारे लिए अथाह प्यार के साथ पल रहीं है कितनी ही चिंताएं /
अनुभव के मांझे को तराश कर उडा देना चाहती हूँ तुम्हारे सभी दुखों को बनाके पतंग (कटें दूसरें लोक में) /
दुः स्वप्नों का रिजर्वेशन ब्रह्माण्ड से परे (माँ कितना गहन सोचती है संतान के हित के लिए पार्वती सा दुर्गा सा )/
चिंताओं को बनाकर हरकारा अनाम अगम्य अचीन्हें पते पर (वाह वाह) /
और समापन की पंक्तियाँ दो टूक सन्देश है बिटिया के लिए देखिये तो …… संस्कार और रूढ़ियों के तले जब भी घुटने लगे सांस मैं मुक्त कर दूंगी तुम्हे उन बेड़ियों से फेंक देना उस छाते को जिसके नीचे रह पाओगी तुम या तुम्हारा सूकून मेरी बेटी।
" मुआवजा" में आदरणीयाj, कविता के बदले बार्टर सिस्टम सा मुआवजा के चलन को मानते हुए कविता के बदले अर्थों की ओर से बेफिक्र होने हेतु मुआवजा मांग बैठती हैं स्त्रियों के आसुओं की कैद का , नए शब्दों का मुआवजा, प्रतिकारस्वरुप निपटने को छलावे और दुःख को; कविताओं में घुस गयी व्यावसिकताओं, तल्खियों, भावनाशून्यता और स्नेहरिक्तता को दूर करने हेतु ताजे मधु का मुआवजा।
" मैं अहिल्या नहीं बनूंगी " में नारी की दमित इच्छाओं का उद्दात्त स्वीकारीकरण, और स्वेच्छाओं का वरण बिना निजत्व (सेल्फ कांसेप्ट) को खोये के भाव को अपनाये रखने की प्रधानता है और तथाकथित मनुओं समाज के ठेकेदारों से शोषित ना होने की पुरज़ोर कामना है, राम की प्रतीक्षा असंदर्भित हो चुकी है आज के बदलते समाज में वाह।
राशन के बिलों पे खपाए लम्हे अन्नपूर्णा का रोल निभाने हेतु , दवाइयां असहमतियां एक्सपायरी होने की तारीखें परिवार को आयुष पोषित करने हेतु , मासूम झूठ, सहमे हुए सच , लेशमात्र बेईमानियां भी और समय असमय परिवार समाज स्वयं से किये गए समझौतों की लिस्ट (वाह)....उनकी कविता परिवार समाज से शुरू होकर वहीं ख़तम होती रही है , इसी लिए नहीं लिख पाती या लिख पायी वो भी एक अदद "प्रेम कविता"।
"बड़े लोग" " दोराहा", "मलाला सिर्फ एक नहीं है" और "कामना" भी काफी अच्छी बन पडी हैं। "वे सिद्ध्हस्त थे आंकने में अनुमानित मूल्य (जीवन मूल्य) जीवन समीकरनों का कि, कितना नीचे गिरने पर कोई बन सकता है कितना अधिक बड़ा। " (और हैं भी, रहेंगे या नहीं वो आज की नयी मलयानिल ने बताना शुरू कर दिया है। ) आजकल की लोलुपता प्रसिद्ध बड़ा होने की अच्छा बुरा कुछ भी करने की और प्रसिद्धि पाने की विवादो से ही सही अगर वादों से नहीं। और " वहाँ एक पगडंडी, कर रही है इंतज़ार नए कदमों का ; तय करो स्री कि आगे दोराहा है " या "किन्तु टूटकर प्यार करने वाली और दीवाना वार हो मजनूं हो जाने वाली तमाम आदिम इच्छाओं के बोझिल पावँ कभी कभी झटकना चाहतें हैं संकोच और जन्मजात संस्कार की बेड़ियां " आदि।
अहिल्या जैंसी भावप्रवणता लिए एक और कविता है " हमें बख्श दो मनु, हम नहीं हैं तुम्हारे वंशज !" इस संग्रह में। गम्भीर चोट है प्रार्थना स्थलों और इबादतगाहों के तथाकथित स्वयंभू ठेकेदारों पर यह अंश "हाशिये पर गए जनेऊ और शिखा नहीं कर पाये दो जून रोटी का प्रबंध , क्योंकि वर्णों के चक्की से नहीं निकलता है जून भर अनाज निकलती है तो केवल लानतें शर्म से झुके सर, बेवजह हताशा और अवसाद। बोझ बनते प्रतीक चिन्हों को नकारते और अनकिये कृत्यों का परिणाम भोगते केवल और केवल कर्मों पर आधारित उनके कल और आज ने सदा ही प्रतिध्वनित किया हमें बख्श दो मनु , हम नहीं हैं तुम्हारे वंशज (वाह वाह)।
क्या है जंगल के उपकार, पानी मिट्टी और बयार। पानी मिट्टी और बयार , जिन्दा रहने के आधार। यह नारा जंगलात के सडकों पर अकेले खड़े साईन बोर्डों पर जहाँ तहां स्कूल जाते पढने को मिलता था हमें जब हम पहाड़ों में १४ - १४ किलोमीटर हाई स्कूल और माध्यमिक कक्षाओं में पढने जाते थे। उसी चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर कवयित्री ने बहुत मार्मिक सही चित्रण किया है; गौरा देवीजी और चण्डी प्रसाद भट्ट जी के वन और पर्यावरण सुरक्षा के प्रयासों का। बानगी देखिये तो ;
" उस रात वे चुन सकती थी /
दिन भर की थकान के बाद सुख और चैन की नींद /
……………तमाम सुविधाओं के उस रात।
……………… उन्होंने चुना जल ,
जंगल और जमीन के उस जागरण को /
……… उन्होंने चुना पेड़ों को जो उनके पिता थे ,
भाई थे, मित्र थे और बच्चे थे। ……………………।
वे अट्ठाइस औरतें सीख गयी द्विगुणित होने की कला" ।
उन्होंने पञ्चतत्व् के चार तत्तवों जल जमीन बयार और वंनस्पति को एक सूत्र में गूंथ लिया था मन की निकली आग और दृढ़ संकल्पों से। मैती होने की सच्ची मिसाल कायम कर दी थी सुदूर चमोली जनपद के सीमान्त अरण्यों में।
"लड़कियां कितनी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं " में माँ बाप रिश्तेदारों और समाज पर तीखा दंश है मसलन। …"कुछ तो गणित रहा होगा रिश्तेदारों के मन में /……स्वर्ग वासी माँ बाप के द्वारा छोड़ी गयी जायदाद की कमाई / यकीनन नोट भरी पड़ गएँ होंगे / तरुणी के रुदन पर। .... हर रोज कितना बूढाईं होंगी वो........
"कद" , "एक स्त्री आज जाग गयी है" और " मेरी माँ "…।
" कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नेक बनने की कीमत चुकाने के लिए/
अधूरा होना क्या पहली शर्त होती है,,,,? जैंसी रचनाओं की परणिति होती है एक और सशक्त रचना में प्रागज्योतिषपुर में घटित अघटित समसामयिक सरोकारों पर लिखी गयी इबारत , शीर्षक है "पब से निकली लड़की" …………
पब से निकली लड़की के /
ताक पर रखते ही अपना लड़कीपना/
सदैव प्रस्तुत होतें हैं 'कचरे' को बुहारते 'समाजसेवी' /
कचरे के साथ बुहारते हुए उसकी सारी मासूमियत अक्सर /
वे बदल जाते हैं सिर्फ आँख और हाथों में ( सिर्फ आँख और हाथों में ) ……
क्या जरूरी है उसके साथ हुए इस व्यभिचार का सनसनी में बदलना /
या ज़रूरी है कैमरा थामे उन ( शायद नपुंसक ) हाथों का आगे बढ़ एक सहारे में बदल जाना"।.………
एक सटीक ज्वलंत प्रश्न है स्नेहशून्य होती संवेदनारहित मानवता के आगे……… कुछ कुछ वह कैमरा वाला हाथ भी वैंसा ही निर्लज्ज नपुंसकीय सोच का स्वामी रहा होगा, जैंसे एक प्रसिद्द फोटोग्राफर जिसने इथोपिया में एक अश्वेत मासूम छोटी लड़की का फ़ोटो खींचना ज्यादा मुनासिब समझा था एक बाज निगाह लगाये जो झपटने को तैयार था भूख से पल पल हड्डी हो चुकी लड़की को। वह फोटोग्राफर खुदकुशी कर गया था महीने बाद आत्मदंश से , लेकिन नैतिकता की चिड़िया यहाँ। चलो छोड़िये भी। "मृत्यु और मेरा शहर" का उद्धरण ध्रुवसत्य मृत्यु के बारे में धर्मराज युधिस्ठिर के उत्तर की याद दिलाता है किरात द्वारा किये गए प्रश्नों के हेतु। (आशाराम बापू के पक्ष में विश्व पुस्तक मेले में बापूजी निर्दोष हैं, की आवाजों पर्चों को सुना था, से भी, करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ और यह जब मैं लिख रहा हूँ, एक और ययाति ने थक हार पुरुरवा को शर्मशार होने से बचा लिया है पता नहीं कब तक ???? (पेज ६१ से ६५ में यह कविता दो बार त्रुटिवश छप गयी है )। " शायद यही एक जरिया है मेरे प्रतिकार का " में अंजू जी चतुर्थ कवितांश में कहती है। ।"एक शहंशाह ................. जीरो ग्राउंड में। वो शायद भूमाफिया हाउसिंग स्वप्नों को बेचते स्वयंभू ठेकेदारों और पहाड़ को चूरा चूरा छोटे छोटे अनगिनत प्रस्तरखंडों में बदलने वाले नदी माफियाओं की तरफ अप्रत्यक्ष रूपेण इंगित कर रही होंगी ?
जहाँ एक और "डर" संक्षिप्त पर प्रभावकारी है। वहीं " आग और पानी " सभी विषमताओं के बावज़ूद भी समरसता और समन्वयक्ता को ढूंढने की कोशिश है नारी द्वारा और सकारात्मक सोच के साथ सम्पन्नता की और बढती हुयी सदा।
"लड़की" आत्मकथ्य है सम्भवतः मुझे तो यही लगा कवयित्री जी। पर वो। .... वो लड़की खोयी नहीं जीवंत है कल्पनाओं से परे के समय में।
सौंपती हूँ तुम्हे
रोशनियों के उस शहर को
जिसके लिए उजाले चुराए हैं तुमने
मेरी आँखों से।
………
जाओ और पा लो खुद को
कर लो वरन अपनी मुक्ति का
और मैं अर्जुन के सहस्त्रों बाणों से बिंधी
प्रतीक्षा करूंगी अपनी मुक्ति की। (मुक्ति)
और
किन्तु
शापित नहीं होना है मुझे
क्योंकि मैं नकारती हूँ
उस विवशता को
जहाँ सदियां गुजर जाती है
एक राम की प्रतीक्षा में, (मैं अहिल्या नहीं बनूंगी )
दोनों विरोधाभासी सी प्रतीत होती हैं पर हैं नहीं अगर गौर से देखें तो मुक्ति में (हताशा से उपजा खिन्न होकर भी) उदारता वाला स्वयं का निर्णय है और अहिल्या में सामाजिक बंधनों से मुक्त होने की छटपटाहट। ("जरूरी काम " सा लीजियेगा इसे भी।) "मै तुम हो जाती हूँ"…… प्रेम अहसासों की कविता है , सुन्दर विम्ब विधान की संयोजना और भावों की पराकाष्ठा से भरपूर अतुकांत काव्य शिल्प से लबरेज।
अंततः !!!
"हम निकल पड़ें हैं", "बंद हुए कश्मीरी बंद प्रगाश के लिए", "भरोषा", "हथियार", "साल १९८४"
और
"यह समय हमारी कल्पनाओं से परे है"
शीर्षक कविता का जिक्र करना चाहूंगा।
हम इतिहास की नीवं का पत्थर हैं किन्तु /
हमारे हर बढ़ते कदम के नीचे से/
खींचे गए बिछे हुए कालीन /
और हर उंचाईं की क़तर ब्योंत को/
जन्मना हक़ समझा गया/
हमसे छीने गए पहचान, नाम और गोत्र तक/
झोली में भरते हुए लाचारगी/
चेहरों पर चिपकाई गयी कृत्रिम मुस्कानें/
सजे धजे हैम बदलतें रहें दुकानों के बाहर खड़े /
३६-२४-३६ के कामुक मेनेकुइन्स में।
हद तो तब हुयी जनाब। ....... सबूत।
भूलने लगे न्यूटन का तीसरा नियम।
जीवन के सापेक्षता के सिद्धांत में /
केवल डूबना ही मायने रखता है/
सिर्फ और सिर्फ खून साफ़ करना/
हमने सीखा एक औरत का तापमान अप्रभावित रहता है सभी कारकों से / (पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज का गणित अंजू जी )
…मांग और पूूर्ति के समस्त नियम /
चरितहीन, मधुबाला, मर्चेंट ऑफ़ वेनिस और पोर्शिया /
अनारकली चांदबीबी मनु और रजिया के अंत के नज़ीर (वाह)
खरपतवार (या पूजा की दूर्वा) या यूकेलिप्टस /
(सबका सुखद अंत होता है सम्भावनाओं के बोलों पर कि)
नकारते हुयें संस्कारों की अफीम (काबिले तारीफ उपमान )
हम निकल पड़ें हैं अपने स्वाभिमान की विजय यात्रा पर।
("हम निकल पड़ें हैं" कविता प्रतीकार्थों से भरी पुस्तकका दूसरा शीर्षक बनाने में भी पूर्णतया सक्षम है। मेरा अपना विचार है आपके निर्णय पर सवाल नही, "जरूरी" को याद करते हुए ) ।
बस तीन कमसिन फूल अब फूलों की घाटी में फिर कभी ना मुस्कराएंगे। (केसर अखरोट खुबानी बागुगोसा सेब की खुश्बू नहीं फैलाएंगे )…
भरोषा शब्दकोष का सबसे क्षतिग्रस्त शब्द है /
भरोषा और धोखा दोनों पूरक शब्द /
भरोषा जितना अधिक होता है उतना ही अधिक होता है धोखे का अनुपात।
भरोशे के बाज़ू से निकल आता है है शक /
और तोलता है तर्क के तराज़ू पर /
भरोशे को /
इंसानियत को/
दोस्तों को।
सूत्रवाक्य "भरोषा" की ही देन हैं। …….
एक पुरुष के भरोशे पर स्त्री रौंप देती है अपने गर्भ में भ्रूण /
भरोशे का कायम रहना दर असल इंसान का कायम रहना है।
(वाह वाह वाह).…………… "हथियार: भी संक्षिप्त लेकिन दमदार है। "साल १८८४" में १९८४ को तो बखूबी आपने कागज़ के कैनवास पर चित्रित कर दिया है सुभान अल्लाह ये कलम की अनवरत यात्रा जारी रहे।
अंत में प्रतिनिधि रचना "यह समय हमारी कल्पनाओं से परे है". .......जिसपर पुस्तक का नामकरण भी हुआ है को स्मृतिपटल पर लाना चाहूंगा। यह समय हमारी कल्पनाओं से परे है. .......
पर हमारी कल्पनाओं से परे,
बहुत परे है
आज के समय की जटिलताएं।
अभिशप्त जीजीविषाएं। …………
मृत प्राय संवेदनाएं
सहज ही ओढ़ लेती हैं उदासीनता का दोशाला
सोच का वृत्त (कोई अंत नहीं जिसका)
सुन्न शिराएँ धीमा रक्त चाप
शिथिल चेतनाएं
(देश निकाला कुटज)
अगर हमारा आज है तप चेत ही जाइये
सचमुच यह समय
हमारी कल्पनाओं से परे,
बहुत परे है.…।
वाकई यह प्रतिनिधि रचना किताब का शीर्षक होने का माद्दा रखती है आपको और प्रकाशक समूह " बोधि " को बधाइयाँ।